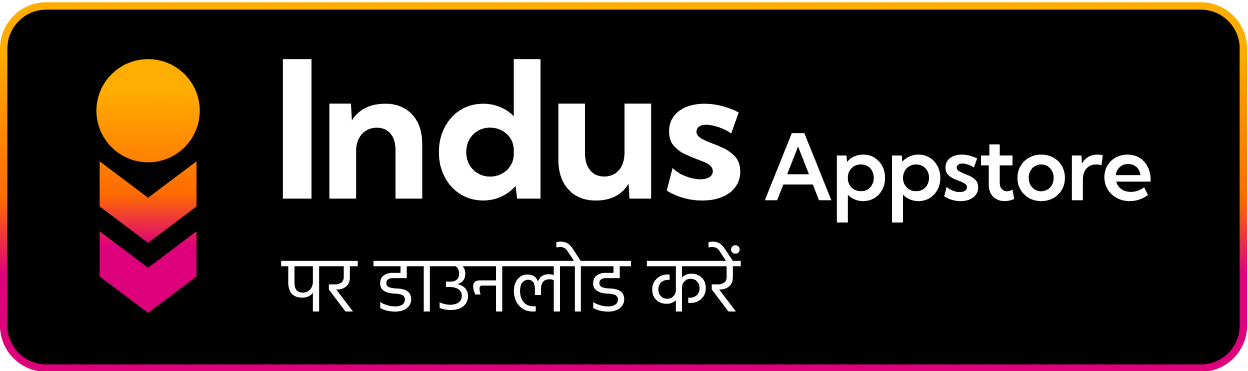अभिमनोज/इंडियामिक्स लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर संवाद है — राज्य और नागरिक के बीच। यह संवाद तब सार्थक होता है जब दोनों पक्षों के अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट, सुरक्षित और न्यायसंगत हों। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि शासन केवल आदेश न दे, बल्कि जनता को यह अधिकार दे कि वह शासन की पारदर्शिता को परखे, उसकी कार्यप्रणाली को समझे, और उसकी जवाबदेही तय करे।
इसी भावना की नींव पर खड़ी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 75 — एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान जो न केवल दस्तावेजों तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करता है, बल्कि लोक सेवकों को यह स्मरण भी कराता है कि वे जवाबदेही के केंद्र में हैं, सत्ता के नहीं।
यह अधिकार कोई हालिया आविष्कार नहीं है। इसकी जड़ें 19वीं सदी के उस कालखंड में हैं, जब भारत ने पहली बार 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से न्याय व्यवस्था को विधिक रूप देना शुरू किया था। उस समय की धारा 76 ने ही नागरिकों को यह अधिकार दिया था कि वे सरकारी दफ्तरों में संग्रहित सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर सकें। इस व्यवस्था को अब नए स्वरूप में, धारा 75 के अंतर्गत यथावत बनाए रखा गया है — यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ अधिकार कालातीत होते हैं; वे सत्ता से ऊपर, और कानून की आत्मा के सबसे करीब होते हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भले ही तकनीकी रूप से नया हो — जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और समकालीन न्यायिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है — पर इसकी धारा 75 उस लोकतांत्रिक दर्शन की निरंतरता है, जो जनता को सिर्फ देख भर लेने की अनुमति नहीं, बल्कि प्रमाणिकता के साथ जानने का अधिकार देती है।
यह प्रावधान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विधिक अधिकार के तहत किसी सार्वजनिक दस्तावेज को देख सकता है, तो संबंधित सरकारी अधिकारी उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उसे देने के लिए बाध्य होगा। यह “बाध्यता” कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी दायित्व है — जिसे टालना, रोकना या अनदेखा करना संविधान के मूल भाव के विरुद्ध है।
यहाँ यह भी समझना होगा कि यह अधिकार, भारतीय संविधान के भाग-III में निहित उन मौलिक अधिकारों से पोषित है, जो प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने, जानने, और संवाद करने का अवसर प्रदान करते हैं। दस्तावेज तक पहुँच इसीलिए महज़ जानकारी नहीं, एक सशक्तिकरण है।
अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब यह अधिकार पहले से ही मौजूद था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) क्यों लाया गया? इसका उत्तर सरल है — RTI ने इस अधिकार को विस्तार, गहराई और संरचना दी। यह अधिनियम केवल दस्तावेज़ी प्रतियाँ नहीं, बल्कि निर्णय की प्रक्रिया, सलाह, फाइल नोटिंग्स, संवाद — सब कुछ माँगने का अवसर देता है। फिर भी, RTI एक अलग उद्देश्य लिए खड़ा है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 एक कानूनी बाध्यता की रीढ़ है — और इसका उल्लंघन सीधे आपराधिक मुकदमे की शक्ल ले सकता है।
RTI अधिनियम, 2005 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 — दोनों का मकसद एक ही है: जनता को सरकारी जानकारी तक पहुँच देना। लेकिन इनके काम करने के तरीके और कानूनी प्रभाव अलग-अलग हैं।
RTI अधिनियम एक विशेष कानून है, जो किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या संस्था से जानकारी माँगने का अधिकार देता है। इसमें आप केवल दस्तावेज ही नहीं, बल्कि निर्णय कैसे लिया गया, किसकी सलाह पर लिया गया, फाइल में क्या-क्या लिखा गया — ये सब भी माँग सकते हैं। इसका उपयोग ज्यादा विस्तृत और व्यापक है।
धारा 75 एक सामान्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जो यह कहता है कि अगर कोई दस्तावेज़ सार्वजनिक है और आप उसे देखने के हकदार हैं, तो सरकारी अधिकारी आपको उसकी प्रमाणित प्रति देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है, तो यह सीधा कानून तोड़ने वाला काम माना जाएगा और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं — एक नागरिक को जानने का अधिकार देता है, दूसरा सत्ता को जवाबदेह बनाता है।
यहीं से यह विषय केवल सूचना की मांग नहीं रह जाता, बल्कि एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न बन जाता है। यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर धारा 75 का पालन नहीं करता, तो वह केवल अपने कर्तव्य से नहीं चूकता, बल्कि जनता के उस अधिकार को नकारता है, जिसकी रक्षा उसका संवैधानिक शपथ है।
इस अवहेलना के दंड भी साधारण नहीं हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act, 2000), और न्यायालयीय निर्देश — सभी इसमें दखल दे सकते हैं। BNS की धारा 172 (पूर्व की IPC धारा 166) ऐसे किसी लोक सेवक पर लागू होती है जो कानूनी कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करता है। यदि कोई अधिकारी न्यायिक आदेशों की अवहेलना करता है, तो BNS की धारा 211 और 212 लागू हो सकती है (पूर्ववत IPC की धारा 187 और 188)। साक्ष्य छिपाने, बदलने या नष्ट करने पर BNS की धारा 236 या उससे संबंधित धाराएं लग सकती हैं। यदि यह कार्रवाई मिलीभगत से होती है, तो BNS की धारा 73 (पूर्व की धारा 120B) के तहत आपराधिक षड्यंत्र का मामला भी बन सकता है।
डिजिटल युग में, जब दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हैं, तो IT Act की धारा 65 और 66 जैसे प्रावधान भी स्वतः लागू हो जाते हैं। कोई अधिकारी यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जानबूझकर नष्ट करता है या उसमें हेरफेर करता है, तो यह सीधे-सीधे दंडनीय अपराध बनता है — जिससे वह केवल अपनी नौकरी ही नहीं, अपना स्वतंत्र भविष्य भी खो सकता है।
इन कानूनी पहलुओं का सबसे बड़ा असर यह है कि अब नागरिक सीधे ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। यह लोकतंत्र की आत्मा को कानूनी अस्त्रों से सज्जित करता है — जिससे जनता केवल शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि साक्ष्य के संरक्षक भी बन जाती है।
न्यायपालिका ने भी इस दिशा में बार-बार स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रशासनिक गैर जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक अपमान है। उच्चतम न्यायालय सहित अनेक उच्च न्यायालयों ने यह दोहराया है कि ऐसी अवहेलना को ‘शून्य सहिष्णुता’ की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसका आशय यह है कि लोक सेवक यदि नागरिकों के सूचना अधिकार में बाधा डालते हैं, तो वे न्याय के कठघरे में खड़े किए जाएंगे — और यह कठोर चेतावनी है।
इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में धारा 75 का महत्व एक रेखा की तरह उभरता है, जो सत्ता को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह वह धारणा है जो शासन और सेवकत्व के बीच अंतर रेखांकित करती है। यह याद दिलाती है कि कोई भी लोक सेवक जनता का स्वामी नहीं, केवल संवैधानिक अनुबंध के तहत कार्यरत प्रतिनिधि है — और उसे उस अनुबंध का पालन करना ही होगा।
यदि कोई अधिकारी इस प्रावधान को हल्के में लेता है, तो यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों में से एक को हिलाने जैसा है। यह कानून केवल शब्दों में नहीं, उसके अनुपालन में जीवित रहता है — और वही अनुपालन लोकतंत्र की साँस है।
अब समय है कि प्रत्येक नागरिक अपने इस अधिकार को जाने, जागरूक रहे, और जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ निर्भीक होकर कानूनी कदम उठाए। और प्रत्येक लोक सेवक यह समझे कि धारा 75 की उपेक्षा केवल कानूनी चूक नहीं, बल्कि नैतिक विफलता भी है। तभी हम उस भारत की ओर बढ़ पाएंगे, जहां सरकारें उत्तरदायी होगी, और नागरिक सच में सशक्त।
यदि कोई अधिकारी धारा 75 के तहत दस्तावेज देने से मना करे तो नागरिक क्या करें?
- पहचानें कि दस्तावेज़ सार्वजनिक है या नहीं
- क्या वह दस्तावेज़ किसी सरकारी कार्यालय में है?
- क्या आपको उसे देखने का वैध अधिकार है (जैसे वह रजिस्टर, रिपोर्ट, ऑर्डर, नोटिस, आदि)?
→ यदि हाँ, तो आप धारा 75 के अंतर्गत उसकी प्रमाणित प्रति पाने के हकदार हैं।
- सरकारी विभाग में लिखित आवेदन दें
- संबंधित कार्यालय को एक आवेदन पत्र दें जिसमें आप धारा 75 के अंतर्गत प्रमाणित प्रति माँगें।
- आवेदन पर दिनांक और प्राप्ति की मुहर लेना न भूलें।
- यदि अधिकारी प्रति देने से मना करे या जवाब न दे
- आप सीधे उसी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत करें।
- इसके बाद भी न मिले तो…
- न्यायिक उपाय अपनाएं
- आप नज़दीकी मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय में आवेदन देकर रिपोर्ट कर सकते हैं कि अधिकारी ने धारा 75 का उल्लंघन किया है।
- आप स्थानीय पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं — क्योंकि यह एक विधिक कर्तव्य से इनकार है, जो आपराधिक श्रेणी में आता है।
- लिखित सबूत ज़रूर रखें
- आवेदन की कॉपी
- प्राप्ति की रसीद या कार्यालय का पत्र
- अधिकारी का नाम, पद और कार्यालय विवरण
धारा 75 और सूचना अधिकार की न्यायिक व्याख्या
(क) State of Uttar Pradesh v. Raj Narain (1975, AIR 865)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा —
“जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य कर रही है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है।”
यह निर्णय सूचना के अधिकार की नींव बना, और आगे चलकर RTI Act का वैचारिक आधार भी।
(ख) S.P. Gupta v. Union of India (1981 Supp SCC 87)
इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायपालिका ने यह टिप्पणी की —
“सूचना तक पहुँच, पारदर्शिता की अनिवार्यता है। सरकार का हर कार्य, जब तक सुरक्षा या राष्ट्रीय हित से सीधा विरोध न हो, जनता की जानकारी में होना चाहिए।”
(ग) Secretary, Ministry of Information & Broadcasting v. Cricket Association of Bengal (1995 SCC (2) 161)
यह फैसला सूचना और विचारों के आदान-प्रदान को मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित करता है।
“सूचना देना, लेना और सार्वजनिक करना — यह सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।”
(घ) Shreya Singhal v. Union of India (2015) 5 SCC 1
धारा 66A को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा —
“कोई भी सूचना, जब तक वह हिंसा या अपराध को स्पष्ट रूप से प्रेरित नहीं करती, तब तक उसे दंडनीय नहीं ठहराया जा सकता।”
(ङ) CBSE v. Aditya Bandopadhyay (2011) 8 SCC 497
यह निर्णय बताता है कि सार्वजनिक संस्थान भी RTI और पारदर्शिता के दायरे में आते हैं।
“जानकारी न देना, किसी व्यक्ति की वैधानिक शक्ति को अपंग करने जैसा है।”
इन सभी मामलों में अदालतों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि सूचना तक पहुँच न केवल एक संवैधानिक हक है, बल्कि एक जनहित में निहित शक्ति है — जिसका उल्लंघन गंभीर विधिक परिणामों को जन्म देता है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं साइबर विधि के अध्येता हैं।)
Website Design By
KAMAKSHI WEB
CONTACT : +91-9753910111